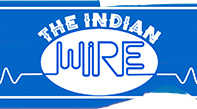Water Crisis In India: पिछले महीने (मार्च-अप्रैल) जब बेमौसम बारिश हुई तो ऐसा लगा कि शायद इस साल गर्मी थोड़ी ठंडक भरी होगी। परंतु जाते हुए अप्रैल ने अपना रंग दिखाया और मई महीने के आगमन के साथ ही सूरज अपने ताप को दिखाना शुरू किया।
इस गर्मी का असर वर्तमान में देश के ज्यादातर हिस्से जबरदस्त गर्मी, लू और तपिश से जूझ रहे है। परंतु इस गर्मी में देश का एक बड़ा हिस्सा जिस विकट समस्या से जूझ रहा है, वह है “पेय-जल संकट”।
भीषण पेय-जल संकट (Drinking Water Crisis) से जूझता ग्रामीण अंचल

समाचार दैनिक दैनिक भास्कर ने आज (16 मई) एक वीडियो अपने वेबसाइट पर साझा किया है। इस वीडियो में कई महिलाएं 70 फीट गहरे कुएं से पानी निकालने को मजबूर है। रिपोर्ट के मुताबिक़ वीडियो महाराष्ट्र के नासिक स्थित पेठ गाँव का बताया गया है। यह इलाका इस वक़्त भयंकर जल-संकट (Water Crisis) से गुजर रहा है।
आपको बता दें, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पानी की ऐसी कमी है कि वहाँ के कई मर्द दूसरी शादी कर रहे हैं। इस दूसरी पत्नि का काम बस गाँव के दूर हिस्से से परिवार के लिए पानी लाना है। इन महिलाओं को “वाटर वाइफ (Water Wife)” कहा जाता है। यह उन सामाजिक अस्थिरता का उदाहरण है जो पानी के संकट के कारण उत्पन्न है और इसमें महिलाओं का शोषण होता है।
दैनिक भास्कर के ही (बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से प्रकाशित) आज (16 मई) के अंक में छपे ख़बर के मुताबिक प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी के कारण हैंडपंप सूख गए हैं। नल-जल योजना की पाइपलाइन तो है, लेकिन पानी नहीं आ रहा। लोगों ने परंपरागत मौसमी जल-स्त्रोतों के आस पास छोटे गड्ढे खोद कर पानी निकालने पर मजबूर है।
बिहार सरकार द्वारा जारी हालिया आर्थिक सर्वेक्षण (2022-23) के मुताबिक राज्य के औरंगाबाद, नवादा, कैमूर, गया, जहानाबाद आदि जिलों में (सभी दक्षिण बिहार संभाग में स्थित) भू-जल स्तर 1 साल के भीतर औसतन 10 मीटर तक नीचे गिरा है।
पर्यावरण और प्रकृति से जुड़े विषय से संबंधित पत्रिका मोंगबे (Mongabay) ने पिछले सप्ताह एक रिपोर्ट में लिखा है कि कैसे भूजल के दोहन के कारण मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले की एक बड़ी आबादी न सिर्फ पेयजल संकट से जूझ रही है बल्कि पानी की कमी का असर वहाँ की कृषि कार्यो पर भारी असर पड़ा है। नतीजतन वहां की आदिवासी बाहुल्य आबादी बेरोजगारी, पलायन और कुपोषण से जूझ रही है।
भूजल दोहन और पेयजल संकट की समस्या महज़ महाराष्ट्र, या छत्तीसगढ़ या बिहार तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है। राजस्थान और गुजरात से पानी की किल्लत की खबरें आये दिन अखबारों में छाई रहती है। देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में अगर 1 दिन भी पानी का टैंकर न पहुँचे तो आलम यह कि हाहाकार मच जाए।
दुनिया के मुक़ाबले भारत में जल-संकट की समस्या ज्यादा विकराल

कुल मिलाकर भारत के कई राज्य इस वक़्त भयंकर जल-संकट (Water Crisis) से गुजर रहे हैं। ड्राफ्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम (DEWS) के अनुसार देश का लगभग 42% हिस्सा सूखाग्रस्त ( Draught Affected) है। पंजाब, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश “सूखा इलाका (Dry-Zone)” माने जाते हैं।
2021-22 में आई कैग रिपोर्ट (CAG Report) के अनुसार पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, और काफी हद तक उत्तर-प्रदेश में लगभग 100 फीसदी भूमिगत जल का दोहन हो रहा है। यूनेस्को (UNESCO) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक़ भारत में पिछले दो दशकों से वर्षा में गिरावट दर्ज की जा रही है। नतीजतन भारत मे कृषि कार्य आदि में भूमिगत जल का उपयोग बढ़ गया है।
हाल में आये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट (UN World Water Development Report 2023) ने बताया है कि 2050 में दुनिया की 1.7-2.4 अरब आबादी जल-संकट से जूझ सकती है जिसका सबसे बड़ा असर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश यानि भारत पर पड़ने वाला है।
वजह साफ़ है। धरती के कुल जल संचय का लगभग 97.3% हिस्सा खारा जल है जो पेय-जल के रूप में सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पृथ्वी के कुल जल संचय का मात्र 2.7% हिस्सा ही स्वच्छ जल माना जाता है। इस स्वच्छ जल में भी ज्यादातर हिस्सा (लगभग 2%) ग्लेशियर, हिमखंड, वातावरण में (जलवाष्प के रूप में) मौजूद है। शेष बचे स्वच्छ जल का भाग ही पेयजल के रूप में इस्तेमाल हो सकता है।
दुनिया मे उपलब्ध कुल पेय जल का मात्र 4% हिस्सा ही भारत मे मौजूद है, जबकि दुनिया की कुल आबादी का 16% भाग भारत मे निवास करती है। जाहिर है, पानी के लिये हाहाकार तो मचना स्वाभाविक है। 1994 में भारत मे पानी की उपलब्धता 6000 घनमीटर प्रति व्यक्ति था, जो वर्ष 2000 में घटकर 2300 घनमीटर प्रति व्यक्ति रह गया। और अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2025 में यह घटकर औसतन 1600 घनमीटर हो जाएगी।
परंतु क्या हम इस खतरे से सचमुच वाकिफ़ हैं? और अगर वाकिफ़ हैं भी तो क्या इसके लिये समुचित उपाय कर रहे हैं? भारत के राजनीतिक दल चुनावों में पानी के बिल तो शहरी क्षेत्रों में माफ़ करने की घोषणा करते हैं; परंतु पानी की उपलब्धता को लेकर इतने सजग और प्रयासरत क्यों नही दिखते?
कहीं बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य हर वर्ष पेयजल संकट से दो चार होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। ग्रामीण अंचल के सुदूर इलाकों के लोग दूषित पानी पीने पर मजबूर हैं।
पानी सभी जीवों के लिए कितना आवश्यक है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन इसके दोहन और इसके बर्बादी से हम बाज नहीं आते। भारत ने अगर समय रहते इन समस्या का निदान न ढूंढा तो आने वाले भविष्य में इसका प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, और पर्यावरणीय कुप्रभाव पड़ेंगे।